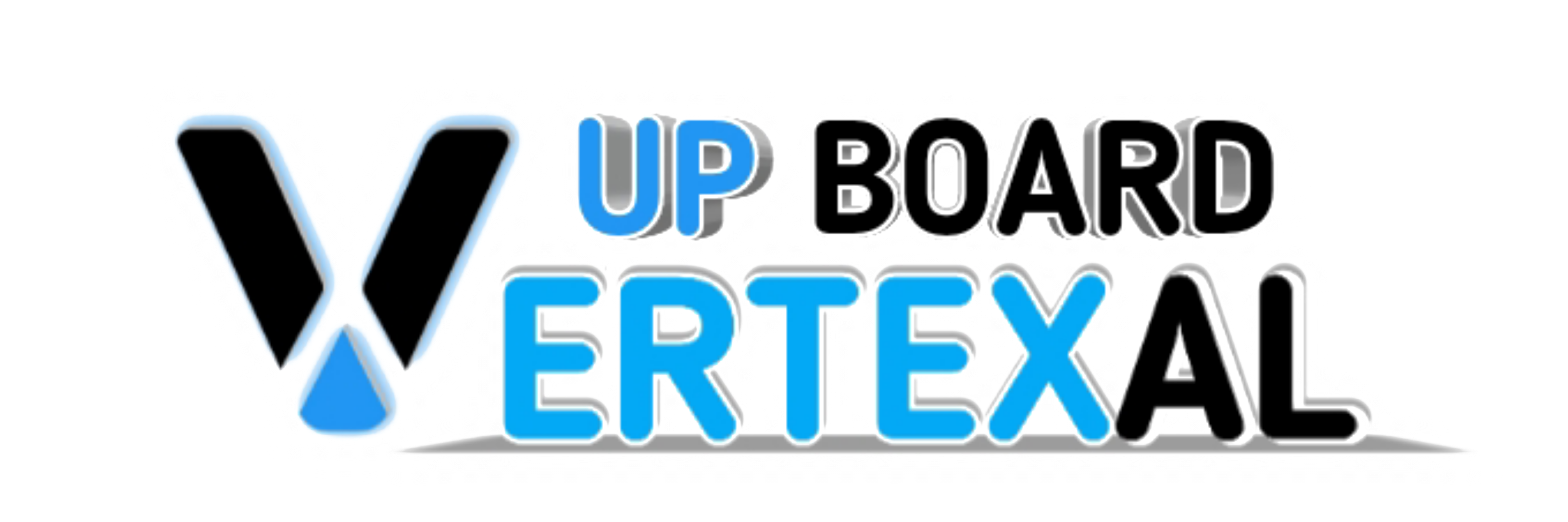अशोक के फूल :आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोतर
1.अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, वह अपूर्व था। सुन्दरियों के आसिंजनकारी नूपुरवाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सौ गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कन्धों पर से ही फूट उठता था।
सन्दर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ‘गद्य गरिमा’ में संकलित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबन्ध ‘अशोक के फूल’ से उधृत है।
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास ने किस प्रकार अपने साहित्य में अशोक का वर्णन करके उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकार बनाया।
व्याख्या लेखक का मानना है कि संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को जो सम्मान दिया वह अपूर्व था। उनसे पहले किसी भी कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया था। अशोक की मादकता का अनुभव करने के लिए कालिदास जैसी दृष्टि आवश्यक है। कालिदास ने अशोक की सुन्दरता का वर्णन किया है। संस्कृत ग्रन्थों मे उसके चामत्कारिक प्रभावों का भी वर्णन किया गया है। उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे, जब कोई अत्यन्त सुन्दर युवती अपने कोमल और संगीतमय नूपुरवाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी।
अशोक के फूलों की सुन्दरता के कारण सुन्दरियाँ उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थीं। यह कर्णफूल जब उनके सुन्दर गालों पर झूलता था तो उनकी सुन्दरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली-नीली चोटी में गूँथती थीं, तो उनकी चंचल लटाओं की सुन्दरता सौ गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। अशोक के कामोत्तेजक गुणों के कारण ही भगवान महादेव के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। इन पुष्पित लताओं को देखकर वियोगी राम के मन में सीता का भ्रम उत्पन्न हुआ था और वह उनका आलिंगन करने के लिए उद्यत हो गए थे। ये काम के देवता मनोज के एक इशारे पर ऊर्ध्वभाग को ऐसा कामोत्तेजक बना देता था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो व्यक्ति के कन्धों से अशोक का वृक्ष फूट उठा हो।
साहित्यिक सौन्दर्य
- (1) भाषा प्रवाहपूर्ण संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। वाक्य विन्यास सुगठित है।
- (ii) शैली विवेचनात्मक है।
- (iii) शब्द शक्ति लक्षणा है।
- (iv) विचार सौष्ठव कालिदास ने अशोक का अतिशययुक्त वर्णन किया है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(1) प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए।
उत्तर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम ‘अशोक के फूल’ है।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या का काले अक्षरों में मुद्रित भाग देखिए।
(iii) प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान् कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है।
(iv) ‘अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, वह अपूर्व था’ पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर ‘अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, वह अपूर्व था’ पंक्ति का आशय यह है कि कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक के फूल को अत्यन्त सम्मान दिया। अशोक के फूल की मादकता का अनुभव करने की दृष्टि कालिदास के पास थी, ऐसा वर्णन अपूर्व (पहले किसी ने नहीं किया) था।
(v) निम्न शब्दों का शब्दार्थ लिखिए आसिजनकारी तथा कर्णावतंस।
उत्तर आसिंजनकारी- अनुरागोत्पादक
कर्णावतंस – कर्णफूल।
2.रवीन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह ! असुर आये, आर्य आये, शक आये, हूण आये, नाग आये, यक्ष आये, गन्धर्व आये, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आयी और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गयी। जिसे हम हिन्दू रीति नीति कहते हैं। ‘वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है’।
सन्दर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ‘गद्य गरिमा’ में संकलित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबन्ध ‘अशोक के फूल’ से उधृत है।
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा उन जातियों का वर्णन किया गया है जो भारत आई और भारतीय सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई।
व्याख्या लेखक ने भारत को विचित्र देश माना है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। लेखक ने यहाँ उन मानव जातियों का वर्णन किया है जो प्राचीनकाल में भारत आई जिनमें असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गन्धर्व आदि के नाम हैं।
यह सभी जातियाँ भारत आई और यहाँ बसी तथा यहाँ से जाने से पूर्व अपनी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गई। इन सभी जातियों व इनकी संस्कृतियों के आगमन से भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का मिश्रण हुआ तथा जनसंख्या को भी विपुलता प्राप्त हुई। रवीन्द्रनाथ ने भारत की जनसंख्या की विशालता को देखते हुए भारतवर्ष को ‘महामानव समुद्र’ की संज्ञा दी। भारत आई इन सभी जातियों का भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान है।
प्राचीनकाल में भारत में जितनी भी मानव जातियाँ भारत आईं उनके भाषा आचार-विचार तथा प्रत्येक कार्यों में भिन्नता थी। किन्तु भारत में आने के पश्चात् इन सभी मानव जातियों की सभ्यता-संस्कृति का यहाँ की सभ्यता संस्कृति में मिश्रण हो गया। और आज हम जिसे हिन्दू रीति-नीति कहते हैं वह हिन्दू रीति-नीति आर्यों तथा भारत आईं विभिन्न मानव जातियों की सभ्यता संस्कृति के उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसमें विभिन्न जातियों की संस्कृति का मिश्रित रूप दृष्टिगोचर होता है।
साहित्यिक सौन्दर्य
- (i) भाषा सरल, सहज और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।
- (ii) शैली वर्णनात्मक है।
- (iii) शब्द शक्ति अभिघा एवं लक्षणा है।
- (iv) विचार सौष्ठव लेखक ने हिन्दू रीति-नीति को भारत में आई विभिन्न मानव-जातियों की सभ्यता संस्कृति के मिश्रण से बनी रीति-नीति कहा है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(i) पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर प्रस्तुत पाठ का शीर्षक ‘अशोक के फूल’ है तथा लेखक का नाम ‘हजारीप्रसाद द्विवेदी’ है।
(ii) रवीन्द्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है?
उत्तर रवीन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी हैं, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र विशाल एवं विस्तृत होता है, उसी प्रकार भारत देश भी लोगों की संख्या की दृष्टि से अत्यन्त विशाल एवं व्यापक है।
(iii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या का काले अक्षरों में मुद्रित भाग देखिए।
(iv) भारतवर्ष के निर्माण में किन-किन का सहयोग रहा है?
उत्तर भारत वर्ष के निर्माण में अनेक जातियों का सहयोग रहा है। असुर, शक, हूण, नाग, आर्य, गन्धर्व आदि प्रमुख ऐसी जातियाँ हैं, जिनका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है और भारतीय संस्कृति के विकास एवं समृद्धि में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।
(v) आर्य, शक, हूण कहाँ आए?
उत्तर आर्य, शक, हूण भारत आए और अपनी संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़ गए। साथ ही भारतीय संस्कृति भी इनका अभिन्न अंग बन गई।
3.कहते हैं, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है! केवल उतना ही याद रखती है, जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है।
सन्दर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ‘गद्य गरिमा’ में संकलित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबन्ध ‘अशोक के फूल’ से उधृत है।
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात् साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है।
व्याख्या लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है, जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वार्थ नहीं सधता है, वह उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बोझिल नहीं होता। समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता, वह उन्हें भूलता जाता है।
किसी वस्तु या व्यक्ति के हाशिए पर जाते ही वह उनकी उपेक्षा करने लगता है। यह सारा संसार विविध प्रकार के स्वार्थों को पूरा करने वाले कार्य-व्यापारों से भरा हुआ एक क्रीड़ा स्थल ही तो है, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाली यह दुनिया अप्रासंगिक चीजों को याद रखकर अपनी ऊर्जा एवं क्षमता का अपव्यय नहीं करना चाहती है।
इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाली इस दुनिया का अशोक के वृक्ष एवं उसके फूल ने कोई स्वार्थ नहीं साधा। यही कारण है कि साहित्यिक वर्ग के प्रबुद्ध लोगों एवं लोकप्रिय रचनाकारों ने अशोक के फूल की उपेक्षा करनी शुरू की और आज उसे पूरी तरह भुला दिया है।
साहित्यिक सौन्दर्य
- (i) भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वाक्य विन्यास सरल तथा सुगठित है।
- (ii) शैली प्रस्तुत गद्यांश की शैली व्याख्यात्मक एवं सूत्रात्मक है।
(iii) शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा है। - (iv) विचार सौष्ठव अशोक को भूल जाने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(i) प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए।
उत्तर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम ‘अशोक के फूल’ है।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या का काले अक्षरों में मुद्रित भाग देखिए।
(iii) प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है?
उत्तर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात् साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है।
(iv) लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है?
उत्तर लेखक ने गद्यांश में उन रचनाकारों या साहित्यकारों को स्वार्थी कहा है, जिन्होंने ‘अशोक के फूल’ के भूल जाने की गलती की है। लेखक के अनुसार संसार बड़ा स्वार्थी है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है।
(v) “सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है।” पंक्ति का क्या आशय है?
उत्तर लेखक कहना चाहता है कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है। उसे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने से फुरसत नहीं है, तो वह अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा, जो शायद उसके लिए किसी काम का नहीं है।
4..मुझे मानव जाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती-बहाती सी जीवन-धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा (जीने की इच्छा) है। वह गंगा की अबाधित-अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण-भर बाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है।
सन्दर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ‘गद्य गरिमा’ में संकलित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबन्ध ‘अशोक के फूल’ से उधृत है।
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य द्विवेदी जी ने मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा-शक्ति के स्वरूप की विवेचना की है।
व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने मनुष्य की जीवनी-शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य जाति के विकास करते जाने के मार्ग को देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीने की इच्छा बड़ी ही अदम्य है, कठोर है, निर्दयी है। वह जीने एवं अपने अस्तित्व की रक्षा करने में अत्यन्त ही कठोर व्यवहार को अपनाता है। वह स्वयं को बचाने के लिए किसी भी अनैतिक एवं क्रूर कार्य को करने से नहीं हिचकिचाता। हजारों वर्षों पूर्व से लेकर अब तक न जाने कितनी जातियों एवं संस्कृतियों की मार्मिक परम्पराओं, रीतियों-नीतियों, विश्वासों एवं उत्सव-व्रतों आदि को समाप्त करती हुई यह आज की स्थिति में पहुँची है। चूँकि मनुष्य कभी भी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रहा। अतः हमेशा ही उसके व्यवहार एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहा है। इसके लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहा। इस प्रयत्नशीलता में ही उसे संघर्ष करने की नई शक्ति मिलती गई और वह उत्तरोत्तर एक नई एवं बेहतर स्थिति की ओर बढ़ता गया। आज समाज का जो रूप है, वह हमें अनेक संघर्षों से प्राप्त हुआ है। आपसी सामंजस्य वस्तुतः अनेक परम्पराओं एवं मूल्यों के बीच समन्वय एवं सन्तुलन का परिणाम है। यह सामंजस्य कई संस्कृतियों की अनेक परम्पराओं एवं उनके मूल्यों को ग्रहण करके तथा अपनी अनेक परम्पराओं एवं मूल्यों को त्याग कर स्थापित हुआ है। आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता सामंजस्य ही है और यह स्वयं में कभी भी विशुद्ध नहीं हो सकता, क्योकि यह तो एक प्रकार का मिश्रण (मेल) ही है। इसीलिए हमारे समाज, देश या जाति की संस्कृति भी विशुद्ध नहीं हो सकती। इसमे मिलावट है। इसमें कई संस्कृतियों के महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तत्त्वों की मिलावट है।
छल-छद्म से परिपूर्ण वर्तमान जीवन में व्यक्ति के आचरण और सभ्यता से लेकर दैनिक उपभोग तक की प्रत्येक वस्तु में किसी-न-किसी प्रकार की मिलावट अवश्य है। संसार में आज यदि कुछ अपने शुद्ध रूप में विद्यमान है तो वह है मनुष्य की प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी जीवित रहने की इच्छा। वह इच्छा आज भी उतनी ही बलवती और आडम्बरहीन है, जितनी कि अपने आदिकाल में थी। यह इच्छा आज भी उसी प्रकार उतनी ही पवित्र है, जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से अपने मार्ग की बाधाओं को समाप्त करके अपने पहले जैसे प्रवाह के साथ निरन्तर गतिशील है और पहले जितनी ही पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह एवं धर्माचार संस्कार कुछ समय के लिए ही इससे टक्कर लेता है, किन्तु मनुष्य की इस दुर्दम जिजीविषा में सब कुछ बह जाता है।
साहित्यिक सौन्दर्य
- (1) भाषा सरल, सहज एवं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास सरल तथा सुगठित है।
- (ii) शैली व्याख्यात्मक एवं सूत्रात्मक है।
- (iii) शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना है।
- (iv) विचार सौष्ठव मानव सभ्यता एक प्रवाहमान धारा के समान है। हमारी सभ्यता और संस्कृति भी अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का मिला-जुला रूप है। इन्हीं तथ्यों की ओर लेखक ने संकेत किया है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(1) प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए।
उत्तर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम ‘अशोक के फूल’ है।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या का काले अक्षरों में मुद्रित भाग देखिए।
(iii) मानव जाति किस मोह को रौंदती चली आ रही है?
उत्तर मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। अब तक न जाने उसने कितनी जातियों एवं संस्कृतियों को अपने पीछे छोड़ दिया है।
(iv) मानव का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है?
उत्तर मानव कभी भी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रहता। अतः हमेशा ही उसके व्यवहार एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहा है।
(v) ‘मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है’ पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर ‘मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है’ पंक्ति का आशय यह है कि व्यक्ति का अपने प्राणों से बहुत मोह होता है। वह सदैव अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता रहता है। यदि अपने प्राणों के लिए उसे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो यह पीछे नहीं हटता, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है तब उसे उचित -अनुचित का ध्यान भी नहीं रहता।
अथवा
मुझे मानव जाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती-बहाती यह जीवन-धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(i) लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है?
उत्तर लेखक को मनुष्य जाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्थात् मनुष्य जाति के विकास करते जाने के मार्ग को लेखक स्पष्ट रूप से देखता है।
(ii) मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है?
उत्तर मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से पाई है। मनुष्य कभी भी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रहा तथा हमेशा ही प्रयत्न शील रहा है। इस प्रयत्नशीलता में ही उसे संघर्ष करने की नई शक्ति मिलती गई और वह नई तथा बेहतर स्थिति की ओर बढ़ता गया।
(iii) ‘धर्माचारों’ और ‘विश्वासों’ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर ‘धर्माचारों’ का अर्थ है किसी धर्म विशेष के आचार और विचार तथा ‘विश्वासों’ का अर्थ है आस्था। मनुष्य की जिजीविषा शक्ति के सम्बन्ध में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं।
(iv) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या का काले अक्षरों में मुद्रित भाग देखिए।
(v) पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर प्रस्तुत पाठ का शीर्षक ‘अशोक के फूल’ तथा लेखक का नाम ‘हजारीप्रसाद द्विवेदी’ है।
5.आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों-सामन्तों ने जिस आचार-निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई; धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह लुप्त हो गया; मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस-राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भाँति उड़ गई, क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक-युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठनृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा-सब नवीन बनेगा।
सन्दर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ‘गद्य गरिमा’ में संकलित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबन्ध ‘अशोक के फूल’ से उधृत है।
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मत है कि सभ्यता और संस्कृति निरन्तर परिवर्तनशील है। समय के प्रहार से कोई नहीं बच सकता।
व्याख्या द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं, वह हमेशा ऐसी ही नहीं बनी रहेगी। सदैव से ही संसार का नियम रहा है कि समय के साथ-साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज जो वस्तु अथवा परम्परा है, वह कल अवश्य परिवर्तित होगी। तब वह एक भिन्न रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होगी। यही बात संस्कृति पर भी लागू होती है। किसी समय सम्राट और सामन्तों ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था, वह अत्यन्त मनमोहक और व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देने वाली थी, पर समय के साथ-साथ एक दिन वह समाप्त हो गई। इसके पश्चात् धर्म के आचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना कीमती समझकर उसकी प्रतिष्ठा समाज में की थी, उसका अस्तित्व भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया। मध्य युग में मुस्लिम शासकों के अनुकरण पर जो रसिक संस्कृति समाज में उमड़ी, वह भी भाप बनकर न जाने कहाँ उड़ गई? अर्थात् समाप्त हो गई।
हमारी वर्तमान संस्कृति भी मध्ययुगीन रसिकता से निर्मित है और वह व्यावसायिक भी है। पर एक दिन इस व्यावसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है, इसके प्रहार से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। एक दिन ऐसा भी आएगा, जब यह धरती रसातल को चली जाएगी। समय की यह विनाशलीला उसकी कुण्ठा के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई कुण्ठाग्रस्त व्यक्ति अपनी ही धुन में, बिना सोचे-समझे कुछ भी करता चला जाता है, उसे सही-गलत का भी ध्यान नहीं रहता, ठीक वैसे ही यह समय भी करता चला जाता है। उसकी मण्डली की प्रत्येक सेविका अपने साथ कुछ-न-कुछ समेट ले जाती है, उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। आज जो नया है, वही कल पुराना हो जाएगा और तब हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा, उसके स्थान पर फिर किसी नवीन वस्तु, विचार का निर्माण करना होगा। सब नवीन बनेगा। भाव यह है कि समय सर्वशक्तिमान है उसके प्रहार से कोई नहीं बच पाता।
साहित्यिक सौन्दर्य
- (i) भाषा सरल, शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। वाक्य विन्यास सरल तथा सुगठित है।
- (ii) शैली विवेचनात्मक एवं सूत्रात्मक है।
- (iii) शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना है।
- (iv) विचार सौष्ठव स्पष्ट किया गया है कि समय निरन्तर परिवर्तनशील है उसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाया है।
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(i) प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए।
उत्तर प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम ‘अशोक के फूल’ है।
(ii) रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या का काले अक्षरों में मुद्रित भाग देखिए।
(iii) धर्माचार्यों के बहुमूल्य ज्ञान-वैराग्य का क्या हुआ?
उत्तर लेखक कहता है कि संसार का नियम है, जो आज जिस रूप में है, कल वह अवश्य नए रूप में परिवर्तित होगा। अतः धर्म के आचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को कीमती व प्रतिष्ठित समझा था, आज उसका अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त हो गया।
(iv) ‘मध्ययुगीन रस-राशि’ से क्या आशय है?
उत्तर मध्ययुगीन रस-राशि से आशय मध्ययुग में मुस्लिम शासकों के अनुकरण से समाज में उमड़ी रसिक संस्कृति से है। लेखक कहता है कि वह संस्कृति भी भाप बनकर कहाँ लुप्त हो गई अर्थात् समाप्त हो गई।
(v) निम्न शब्दों का शब्दार्थ लिखिए मोहक, विकृत ।
उत्तर मोहक आकर्षक, मोहने वाला विकृत – खण्डित